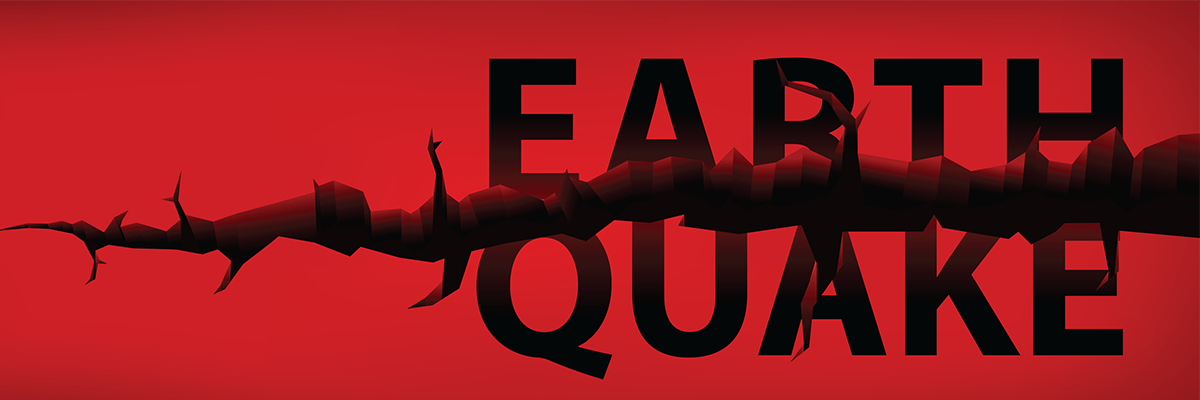आज का मीडिया और नौजवान
– पीयूषकांत राय
अपने समाज की दशा की ओर संकेत करते हुए उरुग्वे के लेखक एडुअर्डो गैलिनो ने लिखा है, “मेरे देश में स्वतंत्रता का अर्थ है राजनीतिक कैदियों के लिए जेल और आतंक । भय पर टिकी शासन व्यवस्थाओं का नाम है जनतंत्र । यहां प्रेम अपनी मोटरगाड़ी से लगाव तक सीमित है और क्रांति का बर्तन धोने के पाउडर की तरह प्रयोग होता है । दक्षिण अमेरिका में एक शांतिपूर्ण देश का मतलब है सुव्यवस्थित श्मशान और स्वस्थ आदमी की पहचान है नपुंसकता ।” क्या ये सब हमारे भारत में होता हुआ नहीं दिख रहा है ? कैसे दिखेगा ? तीन समय में लोगों को नहीं दिखता है ; पहला जब आँखों में आँसू हो, दूसरा जब आँखों में क्रोध की लाली हो और तीसरा जब आँखों में भौतिक विलासिता की खुमारी हो। आँखों से साफ-साफ तभी दिखता है जब हमारा विवेक भी जगा रहता है । विश्व-बाजार की व्यवस्था ने हमसे बहुत कुछ छीना है । उसने हमारी सबसे कीमती चीज विवेक पर डाका डाला है । सन 1947 से पहले भी अंग्रेजों ने हमसे बहुत कुछ छीना । उस समय हमने अपने विवेक को गिरवी नहीं रखा । आज हमने अपना विवेक भी बड़ी-बड़ी कारपोरेट कंपनियों और बाजार के हाथों गिरवी रख दिया है । इसके बदले उन कंपनियों ने हमें अपार संपदा और तमाम भौतिक साजोसामान भीख में दिया है । आजादी से पहले हम इंग्लैंड से पढ़कर आते और अपने देश और समाज के लिए न्योछावर हो जाते । अभी हम अपने देश में सरकारी पैसों (जिसमें गरीबों की भी खून-पसीने की गाढ़ी कमाई का अंश है) से पढ़ते हैं और काबिल बनते ही सबसे पहले अपने देश को छोड़ विदेश में नौकरी के लिए चले जाते हैं । हम विदेश भागने का तर्क यह देते हैं कि भारत में हमारी काबिलियत की अच्छी कीमत नहीं लगाई जाती है । हमारी प्रतिभा की पहचान नहीं है, यहां के लोगों को । यह भी कहते उनका मुंह नहीं दुखता कि अब तो राष्ट्र, देश, भारतीयता जैसी कोई चीज ही नहीं बची । अब कैसा देश प्रेम ? अब तो वैश्वीकरण का जमाना है । अब तो पूरी दुनिया गाँव की तरह है । ग्लोबल विलेज का दौर है । आज के नौजवानों के लिए भारत माँ नहीं है, यह महज एक भौगोलिक सीमा भर है । हमें तो अपनी माँ को भूलते देर नहीं लगती, जिसने बचपन में बिस्तर पर हमारे पेशाब करने के बाद खुद गीले पर सो जाती और हमें सूखे पर सुला देती, ताकि बुखार या सर्दी न लग जाए । यह तो महज माँ के प्रेम का छोटा सा उदाहरण है ।
हम कभी ठहरकर क्यों नहीं सोचते कि हमें इतना पैसा क्यों चाहिए ? अरे मैं तो यह भूल ही गया कि कंपनी तो खुद के मुनाफे के लिए पैसा देती है, न कि हमें ठहर कर अपने या देश-समाज के बारे में सोचने के लिए । हमने तो कसम खाई है कि जो हमें पैसा देगा, उसी के बारे में सोचेंगे । समाज, राष्ट्र, पर्यावरण से हमें सीधे-सीधे कोई आमदनी तो होती नहीं, तो इनके बारे में क्यों सोचें ? हम यह नहीं सोचते कि राष्ट्र ने हमें नागरिकता देने का, समाज ने हमारी सुरक्षा का और पर्यावरण ने पानी और हवा के बदले तो हमसे कुछ वसूला ही नहीं, तो हमारा भी इनके प्रति कोई दायित्व होना चाहिए ।
कभी-कभी लगता है कि आज की शिक्षा केवल लेना सिखाती है, देना नहीं । क्या समकालीन शिक्षा व्यवस्था केवल हमारे अधिकारों के बारे में ही बताती है, कर्तव्यों और दायित्वबोध के पाठ नहीं पढ़ाती । हम भोजन, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, सूचना, इच्छा मृत्यु, समलैंगिकता, बिना विवाह साथ रहने का, जैसे तमाम अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं । राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय संप्रभुता, सामाजिक-आर्थिक समानता, महिला सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, सांप्रदायिकता आदि जैसे मुद्दों के प्रति हमारे क्या-क्या दायित्व और कर्तव्य हैं या होने चाहिए, इसके लिए कोई आंदोलन करने के बारे में सोचते हैं ? ऐसा नहीं सोचते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं हमारी उपभोक्तावादी शिक्षा व्यवस्था की भी बड़ी भूमिका है। आज उच्च शिक्षण संस्थानों में इंजीनियर, मेडिकल, प्रबंधन के गुर तो सिखाए जाते हैं, लेकिन नैतिकता और मनुष्यता के पाठ नहीं पढ़ाये जाते हैं ।
एक वो भी जमाना था, कि हमने रेलगाड़ी और प्रेस, जिन्हें अंग्रेजों ने हमारे दमन के लिए इस्तेमाल करना चाहा, उनका अपनी आजादी के लिए प्रयोग किया । प्रेस की मदद से हमने अखबार निकाले, जिसके जरिए ब्रिटिश हुकूमत की असली मंशा को जनता के सामने रखा । जबकि अंग्रेज़ प्रेस का इस्तेमाल ईसाई मिशनरियों के धार्मिक साहित्य को छापने और उसका भारतीयों के बीच प्रचार-प्रसार में करना चाहते थे, ताकि आसानी से हमें ईसाई बनाया जा सके । हमें अपने-अपने धर्म-मजहब, संस्कृति और साहित्य से दूर रखा जा सके । अंग्रेज़ अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए । हमने उन्हीं के हथियार को उन्हें भारत से खदेड़ने के लिए इस्तेमाल किया । आजाद भारत में इसी अखबार, प्रेस या मीडिया को हमने लोकतंत्र के चौथे खंभे का दर्जा दिया । आज हम इसका सही इस्तेमाल लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं कर पा रहे हैं । हम इसका प्रयोग लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदलने वालों की सुरक्षा और प्रचार-प्रसार में कर रहे हैं । मीडिया लोकतंत्र के चौथे खंभे की भूमिका भले न निभा रहा हो, लेकिन तंत्रलोक का एक मजबूत खंबा जरूर बनता हुआ दिख रहा है। मीडिया कहीं आने वाले समय में महज बाजार के विज्ञापन और ताकतवर तथा निरंकुश मठाधीशों की वीरता और धूर्तता के बखान का माध्यम न बन जाए ! पैसे वालों के लिए मीडिया पर कब्जा करना आसान हो गया है । बाजार में सब कुछ खरीदा-बेचा जा सकता है के तर्ज पर मीडिया और खबर भी बिकाऊ हैं । उम्मीद की किरण अभी भी पुण्य प्रसून वाजपेयी, रविश कुमार आदि के रूप में दिख जाती है, जिसका इन्हें खामियाजा भी कभी-कभी भोगना पड़ता है । पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ठीक ही कहा है कि जो पत्रकार पहले लोकशाही के निगहबान थे, वे अब चारण बन गए हैं । वे लिखते हैं, “जो मीडिया कल तक संसदीय राजनीति पर ठहाके लगाता था वही सत्ता के ताकतवर होते ही अपनी ताकत भी सत्ता के साथ खड़ा होने में ही देखने-समझने लगा है ।” आज मीडिया राजनीति के कृष्ण पक्ष की आलोचना की जगह उससे गले मिलने में अधिक सुख की अनुभूति कर रहा है। मीडिया की अधिकांश खबरों और बालीवुड की अधिकांश फिल्मों को देखकर फिर से सामंतयुग और चारणयुग के भूतों के जिंदा हो उठने का भ्रम होता है । मैं चाहता हूँ यह भ्रम ही रहे, सच न हो जाए । आज बाज़ार और सत्ता ज्यादा निरंकुश हुए हैं । एक बार फिर मीडिया और नौजवानों को अपने कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में सचेत होने का समय आ चुका है ।